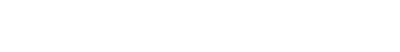योगेंद्र यादव
सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का मतलब बिलकुल साफ है: आरक्षण के सवाल पर न्यायापालिका का रुख पलट गया है और सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक नया दौर शुरू हो गया है।
आजाद भारत में अब तक न्यायपालिका ने आरक्षण के सवाल पर कमोबेश एक इंसाफपसंद रुख अपना रखा था. बेशक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण हिन्दू जजों का वर्चस्व रहा, लेकिन उच्च न्यायपालिका अभी तक अपने सामाजिक पूर्वाग्रहों के बारे में सजग रही थी.
सदियों से चली आ रही जातिगत ऊंच नीच के असर को लेकर संवेदनशील थी. अपने बड़े फैसलों में न्यायपालिका ने संविधान की भावना के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था का अनुमोदन किया था।
लेकिन EWS को आरक्षण देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया ‘जनहित अभियान बनाम भारत सरकार’ फैसले के साथ यह रुझान खत्म हो गया है.
यह फैसला आगे आने वाले खतरे की एक झलक दिखा रहा है क्योंकि बहुमत फैसले में अगड़े और तगड़े वर्ग के आग्रह को संविधान सम्मत सिद्धांतों पर तरजीह दी गई है. जाहिर है न्यायधीशों के अपने सामाजिक परिवेश से मिली धारणाओं और पूर्वाग्रहों का सत्ताधारी विचारधारा से मेल होने से एक वैचारिक बहाव बन रहा है जो संविधान की भावना को पलट सकता है.
अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित हाल में आये फैसलों की तरह अब सामाजिक न्याय के सवाल पर भी अब माननीय न्यायाधीश बहाव के साथ बहने को तैयार ही नहीं तत्पर हैं. विडंबना यह है कि “जनहित अभियान” के मुकदमे में आये फैसले में अदालत ने ‘जन’ और ‘हित’ दोनों को बेमानी कर दिया है.
इस फैसले से एक तरफ सामाजिक न्याय की ताकतों की चुनौती बढ़ गई है तो दूसरी तरफ न्यायपालिका के लिए अपनी पंच परमेश्वर वाली छवि को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है.
आप सोचेंगे कि हम एक छोटे से फैसले से बहुत बड़े निष्कर्ष निकाल रहे हैं. यह फैसला संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम, 2019 की वैधानिकता के बारे में है. इस संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए सामान्य श्रेणी के गरीब उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था.
अदालत की संवैधानिक खंड-पीठ के पांचों न्यायधीश इस सिद्धांत पर एकमत हैं कि आर्थिक परिस्थिति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है. लेकिन बहुमत के तीन और अल्पमत के दो न्यायधीशों के बीच असहमति इस सवाल पर है कि क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के गरीब उम्मीदवार ई.डब्ल्यू.एस कोटा से बाहर रखे जा सकते हैं.
असहमति का फैसला सुनाने वाले दो जजों ने अधिनियम को ‘अपवर्जन और भेदभाव करने वाले सिद्धांत पर आधारित’ कहकर गलत ठहराया है. जबकि खंडपीठ ने अपने बहुमत वाले फैसले में यह कहा है कि जो लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे के अंतर्गत आते हैं उन्हें ई.डब्ल्यू.एस कोटे से अलग करना एक तर्कपूर्ण वर्गीकरण है.
पहली नज़र में यह कानूनी नुक्ते की बारीक कताई का मामला लग सकता है. लेकिन ऐसा है नहीं. अदालत के फैसले में सामाजिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांत की व्याख्या को लेकर जो अन्तर दिखायी देता है वह आरक्षण के सिद्धांत को लेकर लंबे समय से चली आ रही आम सहमति को पलट सकता है.
दशकों से देश की न्यायपालिका ने स्वीकार किया था कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दर्ज समानता के सिद्धांत के अनुरूप है. अदालत की यह सोच विशेष रुप से एन.एम. थॉमस (1976) तथा इंद्रा साहनी (1992) मामले में दिखी. लेकिन अदालत ने हमेशा आरक्षण को एक असाधारण और अंतिम औजार मानते हुए इसके अमल के संबंध में कुछ सख्त शर्ते भी लगायीं थीं.
पहली शर्त यह कि लाभार्थी समूह की परिभाषा तर्कसंगत और स्पष्ट रीति से की जाये. दूसरी बात ये कि जिसे लाभार्थी समूह के रुप में परिभाषित किया गया है वह नुकसान की हालत में है और उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व हासिल नहीं है, इसके ठोस सबूत होने चाहिए ताकि इन सबूतों के आधार पर जरूरी आरक्षण दिया जा सके.
तीसरी बात यह कि आरक्षण की व्यवस्था में अगर कोई फेरबदल की जा रही है तो इस फेरबदल में आरक्षण की निर्धारित अधिकतम सीमा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. इस सिलसिले में अदालत ने एक आखिरी शर्त यह भी जोड़ी थी कि ऐसे किसी बदलाव से ‘गुणवत्ता’ और ‘कार्यदक्षता’ पर ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि उसे स्वीकार नहीं किया जा सके.
हैरानी की बात यह है कि जनहित अभियान मामले में अदालत ने सामान्य वर्ग के EWS को आरक्षण के मसले पर अपने ही बनाए इन चारों सिद्धांतों से मुंह फेर लिया.
बहुमत के फैसले को देखते हुए मन में यही धारणा बनती है कि अदालत को जब ‘उन जैसे लोगों’ के लिए आरक्षण की व्यवस्था देनी होती है तो वह खूब सख्त शर्तें आयद करती है और जब ‘अपने जैसे लोगों’ के लिए आरक्षण देना होता है तो एकदम नरम कसौटी बना लेती है.
पहले जरा परिभाषा से जुड़े मसलों पर विचार कर लें. सभी पांच जज इस बात पर एकमत हैं कि आरक्षण की व्यवस्था का दायरा जाति आधारित पिछड़ेपन से परे भी बढ़ाया जा सकता है.
सिद्धांत रुप में यह बात ठीक लगती है. अगर आपके माता-पिता आपका दाखिला अच्छे स्कूल और महंगे कोचिंग सेंटर में नहीं करवा सकते तो फिर आप उच्च शिक्षा तथा नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता में पिछड़ जायेंगे. इस कमी की भरपायी होनी चाहिए.
लेकिन असल सवाल यह है कि वंचना की इस स्थिति की परिभाषा कैसे की जाये, उसे अमल में कैसे लाया जाये और ऐसे नुकसान की भरपायी के ठीक-ठीक क्या उपाय अपनाये जायें.
खंडपीठ के बहुमत के फैसले में ऐसे महत्वपूर्ण सवालों पर कुछ भी नहीं कहा गया. बहुमत वाले फैसले में बस यह कह दिया गया है कि ‘आर्थिक न्याय भी सामाजिक न्याय के बराबर ही ध्यान का अधिकारी है’ लेकिन फैसले में कहीं भी इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि आर्थिक आधार पर गरीब तबके को आरक्षण देने से क्या विसंगतियां पैदा होंगी.
आर्थिक कठिनाइयां अस्थायी हो सकती हैं और स्वभाव से परिवर्तनशील भी, जबकि खास जाति में जन्म लेने के कारण जो नुकसान उठाने होते हैं वे बड़े गंभीर, स्थायी किस्म के तथा सामाजिक संरचना की उपज होते हैं. ऐसे में दोनों के निदान के लिए एक समान उपाय क्यों अपनाये जायें— अदालत का फैसला यह समझाने में असफल है.
आमतौर पर अदालत जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था पर सख्त निगाह रखती है लेकिन जनहित अभियान वाले मुकदमे में फैसला देते हुए उसने `नुकसान की गंभीरता` वाली कसौटी पर जोर नहीं दिया. मतलब, अदालत का जोर इस बात पर नहीं रहा कि जरा परख लिया जाय कि आरक्षण के अन्य लाभार्थी समूहों को जितनी गंभीर आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं क्या उतनी ही गंभीर आर्थिक कठिनाइयां ई.डब्ल्यू.एस कोटे के लोग भी झेलते हैं.
जांच की एक कसौटी समरुपता (होमोजिनिटी) की भी है जिसमें ये देखा जाता है कि जिन समूहों को लाभार्थी के रुप में चुना गया है वे नुकसान की समान स्थिति में हैं कि नहीं. लेकिन जान पड़ता है अदालत ने इस कसौटी पर भी मामले को परखना जरुरी नहीं समझा.
आर्थिक रुप से कमजोर तबके (ई.डब्ल्यू.एस) की श्रेणी में पर्याप्त विभिन्नता होनी ही है, खासकर आर्थिक स्थितियों के मामले में. इस नाते इस श्रेणी को इंसाफ के तराजू पर तौलने के लिए बड़ा जरुरी है कि आर्थिक रुप से कमजोर तबके के रुप में एक छोटे से वर्ग की पहचान की जाये जो आर्थिक कठिनाइयों के मामले में बड़े हद तक समान हो.
इस वर्ग के निर्धारण की स्पष्टता में जरा सी भी चूक होती है तो गंभीर किस्म का अन्याय सामने आएगा क्योंकि आशंका बनी रहेगी कि कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थतियों के लिहाज से ईडब्ल्यूएस कोटे में शामिल होने का पात्र तो था लेकिन उसे शामिल नहीं किया जा सका.
बड़े अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक निर्बलता के मानक तथा ऐसी निर्बलता की पहचान की कसौटी के सवालों पर विचार करना जरुरी नहीं समझा और इन्हें `वक्त-जरुरत के हिसाब से विचारणीय` मानकर खुला रख छोड़ा है. (अनुच्छेद 96-97, न्यायमूर्ति महेश्वरी).
आइए, अब जरा दूसरी कसौटी यानी सबूतों पर विचार कर लें. अचरज की बात है कि किसी भी फैसले में 10 प्रतिशत के ई.डब्ल्यू.एस कोटे के बारे में यह बुनियादी सवाल नहीं पूछा गया है कि: सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आर्थिक रुप से कमजोर तबके की आबादी कितनी प्रतिशत है?
अगर हम सिन्हो रिपोर्ट को आधार माने—संयोग कहिए कि यही रिपोर्ट मुख्य सबूत हो सकती थी लेकिन बहुमत वाले फैसले में इसका जिक्र तक नहीं आया—तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी के लोगों की संख्या देश की कुल आबादी का 5.4 प्रतिशत है ( गैर एससी/एसटी/ओबीसी आबादी की 30 प्रतिशत की मोटामोटी तादाद में 18 प्रतिशत परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे मान कर की गई गणना).
ऐसे में 10 प्रतिशत का आरक्षण कोटा देने का क्या तुक है? अदालत के बहुमत वाले फैसले में तथ्यगत तथा प्रक्रियागत जरुरतों की भी सुध नहीं ली गई जबकि इस पर अदालत का हमेशा ही जोर रहा है और एम. नागराज (2008) में आये फैसले में कोर्ट ने तथ्यगत तथा प्रक्रियागत जरुरतों को का एक ठोस नीरूपण किया था.
इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने न तो ईडब्ल्यूएस के मौजूदा प्रतिनिधित्व की ही जांच-परख करनी चाही और न ही लक्षित समूह की आर्थिक वंचना का मापन उसे ज़रूरी लगा. जो आंकड़े उपलब्ध थे उनको भी संयम में नहीं लिया गया.
एक तथ्यगत विश्लेषण से पता चलता है कि अगड़ी जातियों के जिस लक्षित समूह को ईडब्ल्यूएस कहा जा रहा है उसका प्रतिनिधित्व उच्च शिक्षा के 445 संस्थानों के छात्रों में पहले से ही 28 प्रतिशत था. ऐसे में उन्हें आरक्षण देने का क्या औचित्य?
तीसरी कसौटी यानी आरक्षण पर आयद अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा को भी राजी-खुशी भुला दिया गया. पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण, अधिसूचित क्षेत्र (शिड्यूल्ड एरिया) में शैक्षिक समता के उपाय, खेतिहर जातियों के लिए कोटा का प्रावधान तथा वंचित धार्मिक समुदाय को आरक्षण देने संबंधित कई सामाजिक नीतियों को कोर्ट ने इसी कारण खारिज कर दिया था कि उनसे आरक्षण की बढ़वार पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन होता है.
ईडब्ल्यूएस के मामले में बचाव का यह तर्क बड़ा थोथा है कि अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पहले से चले आ रही व्यवस्था पर लागू होती है, आर्थिक आधार पर नहीं. संविधान के मूलभूत सिद्धांतों की रोशनी में यह तर्क कहीं टिकता नहीं. यह जाहिर तौर पर दोहरे मानदंड अपनाने का मामला है.
सबसे आश्चर्य की बात है कि चौथी कसौटी यानी इस कोटे का ‘योग्यता’ पर क्या असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण ही फैसले में नहीं आया है. आरक्षण की जब भी बहस होती है, उसके विरुद्ध दुहाइयां अक्सर योग्यता की दी जाती हैं.
लेकिन अदालत के फैसले में योग्यता के तर्क का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है. यह चुप्पी और भी ज्यादा चुभती है जब हम इस तथ्य पर गौर करते हैं कि ई.डब्ल्यू.एस कोटा के लागू होने के शुरुआती दो सालों में इस वर्ग का कट-ऑफ ओबीसी से कम रहा है. जाहिर है, फिर ‘योग्यता’ का तर्क तभी इस्तेमाल किया जाता है जब हम `दूसरों` के बच्चों का जिक्र कर रहे होते हैं, जब बात ‘अपने’ बच्चों को कैपिटेशन फी से हासिल लाभ, उन्हें विदेश में हासिल डिग्री या ईडब्ल्यूएस कोटे से मिले फायदे की आती है तो योग्यता का तर्क हम भूल जाते हैं.
अदालत का स्मृतिलोप और दोहरा मानदंड अनायास नहीं है. इसके पीछे एक सवर्ण जातियों की एक सामाजिक दृष्टि है. न्यायमूर्ति त्रिवेदी तथा न्यायमूर्ति पारदीवाला की जाति-आधारित आरक्षण को समाप्त करने संबंधी टिप्पणी उस दृष्टि को उजागर करती है.
देश की आबादी में महज 20 प्रतिशत लेकिन हर क्षेत्र में 60 से 80 प्रतिशत कुर्सी पर काबिज सवर्ण समाज अब आरक्षित वर्ग को और रियायत देने के मूड में में नहीं है. अब उसका कहना है: या तो आरक्षण बंद करो या फिर हमे भी आरक्षण दो.
यह सड़कछाप तर्क अब अदालत तक पहुंच गया है. हाल के फैसले से विशेषाधिकार सम्पन्न लोगों की सामाजिक दृष्टि में आये बदलाव को कानूनी सिद्धांत का रुप मिल गया है. आरक्षण की व्यवस्था को लेकर भारतीय न्यायपालिका के भीतर बनी एक नाजुक सी सहमति अब टूट रही है.
इस सहमति का आधार था भारत के अभिजन के बीच बड़े न-नुकुर और देरी के बाद पनपा यह स्वीकार-भाव कि देश में जातिगत भेदभाव और असमानताएं मौजूद हैं.
इस स्वीकार-भाव की झलक कई प्रगतिशील फैसलों में दिखायी दी, जैसे टी देवदासन (1964) के मामले में आया जस्टिस सुब्बाराव का फैसला और एन.एम. थॉमस (1976) मामले में बहुमत से आया फैसला. ऐसे प्रगतिशील फैसलों में हाल के कुछ फैसलों का नाम लिया जा सकता है जैसे, बी.के.पवित्रा (2019), सौरभ यादव (2020) और नील ऑरेल्यू नून्स (2022) मामले में आया फैसला.
नवीनतम फैसले से आरक्षण व्यवस्था की वैधता के सामने सवालिया निशान लगा दिया गया है. अगड़ी जातियों के पक्ष में हुई राजनीतिक गोलबंदी से भी कोर्ट की मानसिकता पर असर पड़ा है.
इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे. पिछड़े वर्गों पर आधारित क्षेत्रीय दलों तथा शेष बहुजन समाज के समूहों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आयी हैं उससे संकेत यही मिलता है कि भारतीय न्यायपालिका के जातीय चरित्र को लेकर असंतोष बढ़ना तय है.
जाति जनगणना कराने तथा आरक्षण की अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म करने की मांग के जोर पकड़ने के आसार हैं. जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने और न्यायपालिका को सामाजिक रुप से ज्यादा से ज्यादा समावेशी बनाने की मांग भी जोर पकड़ेगी.
अगर जल्द ही कोई संवैधानिक संस्था अपनी सही न्याय-भावना तथा विवेकपूर्ण दृष्टि के साथ समाधान के लिए आगे नहीं आती तो फिर सामाजिक न्याय के सवाल पर संघर्ष और प्रतिरोध तीखा हो सकता है.
इस फैसले के बाद संवैधानिक पीठ के सदस्यों की जाति को लेकर सार्वजनिक टिप्पणियां हुई हैं, हालांकि ऐसी बात करने वाले यह भूल जाते हैं कि इस फैसले से असहमति जताने वाले दोनो जज न्यायमूर्ति भट्ट और ललित भी सवर्ण हैं।
अगर कोर्ट इसी तरह का फैसला देगा तो उसके लिए ‘जाति न पूछो साधु की’ जैसे तर्क का सहारा लेना मुश्किल हो जायेगा. अगर न्यायपालिका को साधु जैसा मान चाहिए तो उसका आचरण साधु जैसा होना होगा.
अगर आज जजों के जाति-सूचक उपनाम तथा विचारधाराई रुझान उचित और अनुचित टीका-टिप्पणी का विषय बन रहे हैं तो इसकी जवाबदेही स्वयं अदालत की बनती है.
ऐसे में क्या हम यह उम्मीद लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट के नव-नियुक्त मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ एक ‘मर्यादित तथा स्थायी सामाजिक ताने-बाने’ को गढ़ने की घोषित न्यायिक प्रतिबद्धता को साकार कर दिखायेंगे?