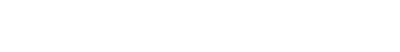**Dr,Qasim Rasool ilyas
( नोट:यह लेख अंग्रेजी अखबार indianexpress में प्रकाशित हुआ है, उसके शुक्रिया के साथ यहां इसे एक परिप्रेक्ष्य के तौर पर पाठकों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है )
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बार फिर उमर खालिद और उसके साथियों की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि मुकदमे में देरी ज़मानत का वैध आधार नहीं हो सकती। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के उस प्रसिद्ध सिद्धांत को और भी कमज़ोर करता है कि “ज़मानत नियम है और जेल अपवाद”। व्यवहार में, खासकर जब अभियुक्त मुस्लिम हों, तो यह सिद्धांत उल्टा काम करता प्रतीत होता है: जेल नियम बन जाता है और ज़मानत अपवाद।
उमर खालिद के लिए, ज़मानत पाने की उनकी यह पाँचवीं नाकामी है। पहले निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज की, उसके बाद उच्च न्यायालय ने भी। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा, तो 14 सुनवाइयों में नौ महीने तक मामला लटका रहा, जिसमें बार-बार स्थगन होता रहा। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तो यहाँ तक दलील दी कि उन्हें बहस के लिए सिर्फ़ 20 मिनट चाहिए, फिर भी अदालत ने उनकी बात नहीं मानी।सामान्य तौर पर, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई स्थगित हो जाती है, तो मामला एक नई बेंच को सौंप दिया जाता है। लेकिन, खालिद के मामले में, मामला लगातार छह सुनवाईयों तक एक ही जज के सामने बार-बार आया। इस स्थिति का सामना करते हुए, उनके वकीलों ने अंततः अपनी याचिका वापस ले ली और निचली अदालतों में फिर से अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। चूँकि बेंच का आवंटन मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि बार-बार बेंच का आवंटन महज संयोग नहीं था। अब, उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में खारिज किए जाने के बाद, एक बार फिर एकमात्र विकल्प सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही है।
इस तरह के मामले एक परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर करते हैं। जब अधिकारियों को पता चलता है कि आरोप कमज़ोर हैं और सामान्य सुनवाई में टिकने की संभावना नहीं है, तो वे गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) जैसे कठोर कानूनों का सहारा लेते हैं। इससे उन्हें आरोपियों को सलाखों के पीछे रखने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आरोपों की गंभीरता अदालतों पर ज़मानत देने से इनकार करने का दबाव डालती है। पिछले दशकों में, टाडा और पोटा ने इसी उद्देश्य को पूरा किया था। आज, यूएपीए और मकोका ने उनकी जगह ले ली है।
हालाँकि यूएपीए मूल रूप से आतंकवाद से जुड़े मामलों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका दायरा छोटे-मोटे अपराधों को भी शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे भी गंभीर बात यह है कि यह न्याय के सिद्धांत को उलट देता है। आमतौर पर, हर आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। इसलिए ज़मानत एक स्वाभाविक अधिकार है। हालाँकि, यूएपीए के तहत, सबूत पेश करने का भार बदल जाता है: ज़मानत के चरण में ही, आरोपी को यह साबित करना होता है कि वह निर्दोष है। वास्तव में, किसी भी वास्तविक मुकदमे के शुरू होने से पहले एक छोटा-सा मुकदमा चल जाता है।मामले को और भी बदतर बनाने के लिए, अभियोजन पक्ष भारी-भरकम आरोप-पत्र दायर करता है—अक्सर हज़ारों पन्नों के—और फिर कई पूरक आरोप-पत्र भी जोड़ देता है। इससे कार्यवाही में इतनी देरी हो जाती है कि अगर आरोपी अंततः बरी भी हो जाता है, तो भी वह अपने जीवन के सबसे कीमती साल जेल में बिताता है। इस प्रकार, बिना दोषसिद्धि के, राज्य किसी भी सज़ा से भी कठोर सज़ा देने में कामयाब हो जाता है: समय और आज़ादी की धीमी चोरी।
ऐसे कानून भारतीय संविधान की मूल भावना पर प्रहार करते हैं। अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। फिर भी, यूएपीए के तहत, यह अधिकार निरर्थक हो जाता है।
यहाँ तक कि जब 15 या 20 साल बाद किसी आरोपी को बरी कर दिया जाता है, तब भी उन पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों की कोई जवाबदेही नहीं होती जिन्होंने सबूत गढ़े और ज़िंदगियाँ बर्बाद कीं। तब तक, पीड़ित अक्सर इतना टूट चुका होता है—शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से—कि वह एक और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं रहता। अदालतें भी मुआवज़े की कोई गुंजाइश नहीं छोड़तीं, और आमतौर पर फ़ैसलों को इस तरह के शब्दों के साथ समाप्त करती हैं: “अपराध भले ही हुआ हो, लेकिन अपराध साबित करने के लिए सबूत अपर्याप्त हैं।” अदालतें शायद ही कभी यह स्वीकार करती हैं कि सबूत गढ़े गए थे या अभियुक्त को जानबूझकर फँसाया गया था। खोए हुए वर्षों के लिए मुआवज़ा लगभग कभी नहीं दिया जाता।
गहरा सच यह है कि ये कठोर कानून राजनीतिक हथियार हैं। सरकारें, चाहे किसी भी दल की हों, विरोधियों को चुप कराने, कार्यकर्ताओं को दबाने और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करती रही हैं। कांग्रेस ने 1967 में यूएपीए लागू किया था और 2008 में, गृह मंत्री पी चिदंबरम ने 26/11 के मुंबई हमलों के बाद पोटा के कठोर प्रावधानों को शामिल करके इसका दायरा बढ़ाया। आज, भाजपा यूएपीए का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है, खासकर मुसलमानों और असहमति जताने वालों के खिलाफ।
भारत के नियमित आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) – पहले से ही आतंकवाद सहित अपराध से निपटने के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करते हैं। यूएपीए जैसे असाधारण कानून पुलिस और सरकार को केवल अनुपातहीन शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जिनका लगभग अनिवार्य रूप से दुरुपयोग होता है। इससे भी बदतर, इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई जवाबदेही तंत्र मौजूद नहीं है।
टाडा (1985-1995) का इतिहास एक भयावह याद दिलाता है: गिरफ़्तार किए गए 67,000 लोगों में से एक प्रतिशत से भी कम को दोषी ठहराया गया। बड़े पैमाने पर प्रतिरोध के बाद पोटा का भी यही हश्र हुआ, लेकिन अनगिनत ज़िंदगियाँ बर्बाद करने से पहले नहीं। यूएपीए और मकोका अब नए नामों से इसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।किसी भी लोकतंत्र में ऐसे कानूनों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों और मानवीय गरिमा को कुचलते हों। ये कानून न्याय को उलट देते हैं, असहमति को अपराध बनाते हैं और संविधान के मूल सिद्धांतों को ही नष्ट कर देते हैं।
आज समय की सबसे बड़ी ज़रूरत एक नए जन आंदोलन की है – ठीक वैसे ही जैसे भारत कभी टाडा और पोटा के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था – जब तक कि यूएपीए और अन्य क्रूर कानूनों को इतिहास की गर्त में न धकेल दिया जाए। तभी हम इस विश्वास को पुनः स्थापित कर सकते हैं कि विलंबित न्याय, न्याय से वंचित न हो जाए।
लेखक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) और उमर खालिद के पिता हैं। यह लेखक के निजी विचार है (अंग्रेजी से अनुवाद) courtesy Indian express